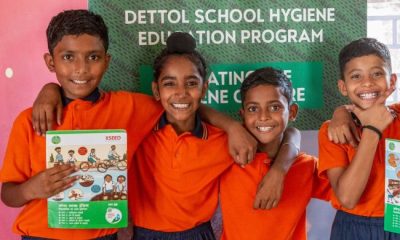नई दिल्ली: खाद्य उत्पादन और भोजन विकल्पों का पर्यावरण पर गहरा असर पड़ता है और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में काफी योगदान होता है, जो जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज का कारण बनता है. यह क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों से बुरी तरह प्रभावित हुआ है. खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) का कहना है कि जलवायु परिवर्तन वैश्विक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, गरीबी उन्मूलन और सतत विकास हासिल करने की हमारी क्षमता को खतरे में डाल रहा है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मानवीय गतिविधियों के चलते दुनिया भर में होने वाले उत्सर्जन (ग्लोबल इमिशन) का 31 फीसदी हिस्सा कृषि खाद्य प्रणालियों (एग्री फूड सिस्टम्स) के चलते होता है. ग्रीनहाउस गैसों की बढ़ती मात्रा वातावरण को गर्म करती जा रही है, जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन रही है. विश्व बैंक की 2020 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग दुनिया में 690 मिलियन लोग (दुनिया की कुल आबादी का 8.9 फीसदी) भूखे हैं, पिछले पांच वर्षों में इनकी तादाद में लगभग 60 मिलियन की वृद्धि हुई है. रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि आने वाले वर्षों में खाद्य सुरक्षा चुनौती और अधिक कठिन हो जाएगी, क्योंकि दुनिया को करीब 9 अरब लोगों को खिलाने के लिए 2050 तक लगभग 70 प्रतिशत अधिक भोजन का उत्पादन करने की आवश्यकता होगी.
जलवायु परिवर्तन के प्रति कृषि की अत्यधिक संवेदनशीलता के कारण चुनौती और भी बढ़ गई है. बढ़ते तापमान, मौसम में बदलाव, कृषि पारिस्थितिकी तंत्र की सीमाओं में बदलाव, आक्रामक फसलों व कीटों और अधिक लगातार मौसम की चरम स्थितियों के रूप में जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव पहले से ही देखने को मिल रहे हैं. जलवायु परिवर्तन से खेतों में फसलों की पैदावार, अनाजों की पोषण संबंधी गुणवत्ता और मवेशियों की उत्पादकता भी घटती जा रही है.
इसे भी पढ़े: बच्चे और वायु प्रदूषण: जानिए बच्चों को वायु प्रदूषण से होने वाले प्रभाव से कैसे बचाएं
दुनिया के विभिन्न देशों के नेता जलवायु परिवर्तन पर सीओपी 28 वार्ता के लिए दुबई में एकत्र हुए हैं. इस बीच ‘बनेगा स्वस्थ इंडिया’ ने हमारे दैनिक जीवन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझने की अपनी सीरीज के तहत यूएनडीपी इंडिया के एक्शन फॉर क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट के प्रमुख आशीष चतुर्वेदी से बात की. उनके साथ लोगों का जीवन, हवा (जिसमें वे सांस लेते हैं) से लेकर पानी और भोजन तक पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा की.
चतुर्वेदी ने फसलें उगाने के तरीके में जलवायु परिवर्तन के मुताबिक सुधार लाने और सभी के लिए भोजन और पोषण की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बारे में संवाद करने का निर्णय लिया.
क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की मूल बातें समझाते हुए और भारत एक हरित परिवर्तन (ग्रीन स्विच) कैसे कर सकता है, की चर्चा करते हुए चतुर्वेदी ने कहा,
हम पहले से ही जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभावों का सामना कर रहे हैं, वर्षा और बारिश के पैटर्न में बदलाव आ रहा है. हमारी कृषि पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि यह मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है. इसलिए, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का मूल रूप से मतलब उन प्रक्रियाओं और तरीकों से है, जिन्हें क्षेत्र के भीतर अपनाए जाने की आवश्यकता है, यह जलवायु परिवर्तन के संकट से निपटने में मदद करेगा. यह जानने से लेकर कि किसी को कौन से बीज बोने चाहिए, उन्हें किस समय उगाया जाना चाहिए और किस प्रकार की फसलों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर ऐसी चीजों का एक सेट है जिन्हें जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपनाने की आवश्यकता है. यह कृषि क्षेत्र से उत्सर्जन (इमिशन) को कम करने से भी संबंधित है, जो कि ग्रीन हाउस गैसों के लिए जिम्मेदार है. खासकर धान जैसी फसलें हमारी जलवायु के लिए बहुत नुकसानदायक हैं. इस तरह, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर जलवायु परिवर्तन को अपनाने, नई पद्धतियों और उन प्रथाओं को अपनाने के बारे में है, जो कृषि क्षेत्र से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने में मददगार हों.
क्लाइमेट स्मार्ट खेती किस तरह भारत को प्रदूषण के बोझ को कम करने में मदद करेगी, इस बात पर प्रकाश डालते हुए चतुर्वेदी ने कहा,
खेती हवा, पानी और भूमि प्रदूषण जैसी चीजों से जुड़ी हुई है. यदि आप समझदारी से खेती करते हैं, तो आपको कीटनाशकों और रसायनों के उपयोग पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी, जो हमारी भूमि को काफी नुकसान पहुंचाते हैं और जब पानी में इनका रिसाव होता है, तो यह हमारे जल स्रोतों को काफी नुकसान होता है. इसलिए, यदि जलवायु के अनुकूल पद्धतियों को कुशलता पूर्वक लागू किया जाए, तो इसका हमारे पूरे पर्यावरण पर सकारात्मक असर देखने को मिलेगा.”
भारत इस बड़े बदलाव के संबंध में देश जो कुछ कर रहा है, उसके बारे में बात करते हुए चतुर्वेदी ने कहा,
अच्छी बात यह है कि भारत सरकार जलवायु परिवर्तन के मुद्दे और कृषि पद्धतियों के धरती पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर काफी जागरूक है. दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में एक बड़ी आबादी कृषि क्षेत्र पर निर्भर करती है. इसलिए क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की पद्धतियों को अपनाने और छोटे किसानों के हित के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है. भारत सरकार ने इसे लेकर कृषि में राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु के प्रति संवेदनशील प्रथाओं को शुरू करने के लिए नेशनल क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव जैसी कई पहल शुरू की हैं. हमारे पास गोबरधन योजना भी है, जिसके तहत पशु अपशिष्ट का उपयोग बायोगैस बनाने में किया जा रहा है. ये कुछ उदाहरण हैं, जो इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि भारत कैसे अग्रणी भूमिका निभा रहा है और कृषि को ज्यादा पर्यावरण अनुकूल बना रहा है.
चतुर्वेदी ने जलवायु हितैषी कृषि पद्धतियों के बारे में किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को जागरूक करने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि यह किसानों और सरकार के बीच दो-तरफा संवाद पर निर्भर है. उन्होंने आगे कहा,
किसान परंपरागत रूप से पर्यावरण के अनुकूल खेती के तौर-तरीकों को लेकर जागरूक रहे हैं, साथ ही उन्होंने उन नीतियों को भी अपनाया है, जो सरकार की ओर से उन्हें बताई गई हैं. उदाहरण के लिए, देश के कुछ हिस्सों में चावल और गेहूं का फसल चक्र उन फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर टिका होता है, जिसका पर्यावरण पर प्रभाव पड़ सकता है. इसलिए सारी जिम्मेदारी अकेले किसानों पर डालना अनुचित है. मुझे लगता है कि क्लाइमेट स्मार्ट खेती के लिए बदलाव लाने में नीतियां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. भारत अब बाजरे की खेती बढ़ाने पर भी ध्यान दे रहा है, जो एक जलवायु के अनुकूल फसल भी है. आज सरकारी नीतियों को जमीन पर उतारने के लिए बेहतर समन्वय की जरूरत है. हमारे पास एक सक्षम कृषि मंत्रालय है, मजबूत वितरण तंत्र है, हमें केवल जागरूकता और कार्यान्वयन की आवश्यकता है, ताकि सारी चीजों को एक साथ आगे बढ़ाया जा सके.
अंत में, इससे जुड़ी चुनौतियों और आगे की राह का जिक्र करते हुए, चतुर्वेदी ने कहा,
लोगों और किसानों को नई चीजें अपनाने के लिए राजी करना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन मुझे यह भी लगता है कि यदि आपके पास राजनीतिक इच्छाशक्ति है और सुधारों और क्लाइमेट स्मार्ट तरीकों को लागू करने के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता कार्यक्रम चलाकर इस संदेश को घर-घर पहुंचाने और इस अभियान की रफ्तार बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए जाते हैं, तो पर्यावरण में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है.
इसे भी पढ़े: जानिए बढ़ते वायु प्रदूषण का आपके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है और इससे खुद को कैसे बचाएं