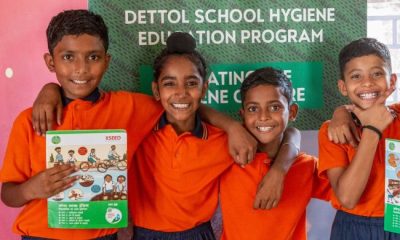नई दिल्ली: जलवायु परिवर्तन पर ग्लासगो में चल रहे 26 वें संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन COP26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में, जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते में हुई सहमति से जुड़ी बातों को आगे बढ़ाने के लिए भारत की जलवायु परिवर्तन कार्य योजनाओं को निर्धारित करने बर बात की. भारत और दुनिया के कई अन्य हिस्सों में, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पहले से ही मौसम की चरम घटनाओं के रूप में दिखाई दे रहा है जैसे कि रिकॉर्ड बरसात, बाढ़, जंगल की आग, भूस्खलन, सूखा, चक्रवात, अन्य. यूके में चल रहे जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी द्वारा घोषित जलवायु कार्य योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
– 2070 तक नेट-जीरो हासिल करना
– अब 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में एक अरब टन की कमी करना
– 2030 तक अक्षय ऊर्जा घटक को देश की कुल ऊर्जा जरूरतों के 50 फीसदी तक बढ़ाना
– 2030 तक कार्बन की तीव्रता को 45 फीसदी तक कम करना
– गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर 2030 तक 500 गीगावॉट तक पहुंचाना
– 2030 तक भारतीय रेलवे को नेट जीरो बनाना
एक प्रदूषक के रूप में कहां खड़ा है भारत?
एक वैज्ञानिक ऑनलाइन प्रकाशन ‘अवर वर्ल्ड इन डेटा’ के अनुसार, जो गरीबी, बीमारी, जलवायु परिवर्तन जैसी बड़ी वैश्विक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करता है, भारत तीसरा सबसे बड़ा ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जक है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद वैश्विक उत्सर्जन के 7.18 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार है. (यूएसए) जो वैश्विक उत्सर्जन का 14.48 प्रतिशत उत्पादन करता है और चीन जो 2019 के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक उत्सर्जन के उच्चतम 27.9 प्रतिशत के लिए जवाबदेह है.
अगर यूरोपीय संघ (28 सदस्यों के साथ) पर विचार किया जाए, जो वैश्विक उत्सर्जन का 9.02 प्रतिशत उत्पादन कर रहा है, तो भारत चौथा सबसे बड़ा जीएचजी उत्सर्जक है.
‘अवर वर्ल्ड इन डेटा’ के अनुसार, 2019 में (सबसे हालिया डेटा उपलब्ध), दुनिया ने कुल मिलाकर 36.44 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) उत्सर्जित किया. इसमें से चीन का हिस्सा 10.17 बिलियन टन, यूएसए ने 5.28 बिलियन टन, EU-28 ने 3.29 बिलियन टन और भारत ने 2.63 बिलियन टन CO2 उत्सर्जित किया.
उत्सर्जन कटौती लक्ष्य भारत ने पहले वादा किया था और स्थिति
भारत ने वैश्विक स्तर पर जिन जलवायु लक्ष्यों की घोषणा की है, उन्हें मोटे तौर पर 2020 से पहले के लक्ष्यों और पेरिस समझौते (COP21) के तहत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) में किए गए वादों में विभाजित किया जा सकता है.
इसे भी पढ़ें: साफ दिख रहा जलवायु परिवर्तन, अस्तित्व के लिए खतरा है: पर्यावरणविद् सुनीता नारायण
2020 से पहले का जलवायु लक्ष्य
जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के अनुसार, 2020 से पहले की वैश्विक जलवायु कार्रवाई में क्योटो प्रोटोकॉल (2008-12) और क्योटो प्रोटोकॉल में दोहा संशोधन (2013-20) के तहत वादा किए गए मात्राबद्ध ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी के प्रयास शामिल हैं.)
भारत ने 2020 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी की प्रत्येक इकाई के लिए उत्सर्जित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की कुल मात्रा) की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 20-25 प्रतिशत कम करने का संकल्प लिया था. संयुक्त राष्ट्र जलवायु सचिवालय को प्रस्तुत अपने तीसरे द्विवार्षिक अद्यतन में फरवरी में, भारत ने बताया कि 2016 में उत्सर्जन की तीव्रता 2005 के स्तर से 24 प्रतिशत कम थी.
पेरिस समझौते के तहत एनडीसी
COP21 के दौरान 2015 में पेरिस समझौता अपनाया गया था. हस्ताक्षरकर्ता देशों ने एनडीसी प्रस्तुत किए जो पेरिस समझौते के तहत इन देशों द्वारा की गई प्रतिबद्धताएं हैं. COP21 के दौरान यह सहमति हुई थी कि पेरिस समझौता 2021 से शुरू होगा. UNFCCC के अनुसार, COP26 के दौरान पेरिस समझौते के लिए नियम पुस्तिका को अंतिम रूप दिया जाएगा.
भारत के 2015 एनडीसी में निम्नलिखित आठ लक्ष्य शामिल थे, जिनमें से तीन में दस साल की समय सीमा के लिए मात्रात्मक लक्ष्य हैं:
– परंपराओं और संरक्षण और संयम के मूल्यों के आधार पर एक स्वस्थ और टिकाऊ जीवन शैली का प्रचार करना.
– आर्थिक विकास के अनुरूप स्तर पर अब तक दूसरों द्वारा अपनाए गए मार्ग की तुलना में जलवायु के अनुकूल और स्वच्छ मार्ग अपनाना.
– 2005 के स्तर से 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 33 से 35 प्रतिशत तक कम करना.
– 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन बेस्ड ऊर्जा संसाधनों से तकरीबन 40 फीसदी संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता प्राप्त करना.
– 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्षों के आवरण के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाना.
– जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों, विशेष रूप से कृषि, जल संसाधन, हिमालयी क्षेत्र, तटीय क्षेत्रों, स्वास्थ्य और – आपदा प्रबंधन में विकास कार्यक्रमों में निवेश बढ़ाकर जलवायु परिवर्तन के लिए बेहतर अनुकूलन करना.
– जरूरी संसाधन और संसाधन अंतराल को देखते हुए उपरोक्त शमन और अनुकूलन कार्यों को लागू करने के लिए विकसित देशों से घरेलू और नए और अतिरिक्त धन जुटाना.
– क्षमताओं का निर्माण करने के लिए, भारत में अत्याधुनिक जलवायु प्रौद्योगिकी के तेज प्रसार के लिए एक घरेलू ढांचा और अंतरराष्ट्रीय वास्तुकला तैयार करना और ऐसी भविष्य की प्रौद्योगिकियों के लिए संयुक्त सहयोगी अनुसंधान एवं विकास के लिए.
इसे भी पढ़ें: जलवायु परिवर्तन के समाधानों को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश की 27 साल की वर्षा ने लिया रेडियो का सहारा
MoEFCC के अनुसार, भारत दो मात्रात्मक लक्ष्यों- उत्सर्जन तीव्रता में कमी और गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित बिजली उत्पादन क्षमता की हिस्सेदारी के लिए 2030 के लक्ष्यों को पार करने की राह पर है.
सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) के अनुसार, देश ने पहले ही 2005 के स्तर से नीचे जीडीपी में उत्सर्जन की तीव्रता में 25 प्रतिशत की कमी को 2005 के स्तर से कम कर दिया है.
विद्युत मंत्रालय के अनुसार, जुलाई 2021 तक, भारत में गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों की उत्पादन क्षमता का 38.5 प्रतिशत हिस्सा है और 2023 तक 40 प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद है. भारत ने अक्षय ऊर्जा के 101 गीगावाट से अधिक की क्षमता स्थापित की है. नवंबर 2021 तक ऊर्जा और 2030 तक 500 गीगावाट स्थापित करने का लक्ष्य है.
डी. रघुनंदन, वैज्ञानिक और दिल्ली साइंस फोरम के सदस्य कहते हैं. ”हालांकि, एक अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने के तीसरे मात्रात्मक लक्ष्य की स्थिति, जो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने वाले जंगलों जैसे प्राकृतिक शरीर को संदर्भित करती है, से संबंधित है.”
यह धीमी प्रगति वनीकरण प्रयासों और बड़े पैमाने पर वनों की कटाई के कारण है, उन्होंने कहा. ग्लोबल फ़ॉरेस्ट वॉच द्वारा किए गए एक अनुमान के अनुसार, मैरीलैंड विश्वविद्यालय, गूगल, यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे और नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) के बीच एक सहयोग, भारत ने 2001 और 2020 के बीच वृक्षारोपण के अपने प्राथमिक वनों का 18 प्रतिशत और अपने का 5 प्रतिशत खो दिया.
उत्सर्जन पर अंकुश लगाने के लिए भारत द्वारा की गई कार्रवाई
– 2008 में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) शुरू की गई, जिसमें सौर ऊर्जा के क्षेत्रों में लक्ष्य, ऊर्जा दक्षता में वृद्धि, स्थायी आवास, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखना, हरित भारत, सतत कृषि और जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान शामिल हैं.
– इमारतों में ऊर्जा दक्षता में सुधार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक परिवहन में बदलाव के माध्यम से शहरों को टिकाऊ बनाने के लिए 2010 में स्थायी आवास पर राष्ट्रीय मिशन (NMSH) लागू किया गया. NMSH में कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (AMRUT) योजना, स्मार्ट सिटी मिशन, विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना (हृदय) योजना, स्वच्छ भारत मिशन आदि का कार्यान्वयन शामिल है.
– उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन (NMEEE) जिसे 2011 में भवन दक्षता और टिकाऊ परिवहन को शामिल करने के लिए लागू किया गया था.
– हरित भारत मिशन (जीआईएम) 2014 में 5 मिलियन हेक्टेयर पर वन/वृक्ष आवरण बढ़ाने और अन्य 5 मिलियन हेक्टेयर पर वन आवरण की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए शुरू किया गया था. जीआईएम ने 2015 से 2019 की समयावधि के दौरान 96,895 हेक्टेयर के लक्ष्य क्षेत्र में से 76,117 हेक्टेयर क्षेत्र में वनरोपण किया है.
– 122 शहरों में 2017 की तुलना में 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) 2.5 प्रदूषण को 20-30 प्रतिशत तक कम करने के उद्देश्य से स्वच्छ वायु कार्य योजना तैयार करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी), 2019 को अपनाया गया.
– इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने के लिए नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान (NEMMP) 2020 लॉन्च किया गया.
– राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, 2021 में घोषित किया गया. पहली हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइज़र निर्माण इकाई इस साल अगस्त में बेंगलुरु में स्थापित की गई थी. इलेक्ट्रोलाइजर वह प्रणाली है जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस या पानी का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में स्लिटिंग किया जाता है.
– बढ़ते वैश्विक तापमान और भारत के जलवायु वादों के बारे में NDTV से बात करते हुए, इंटरनेशनल फोरम फॉर एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी (iFOREST) के सीईओ चंद्र भूषण ने कहा,
”वैश्विक औसत सतह का तापमान 2020 में पूर्व-औद्योगिक औसत से 1.2 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंच गया, और चेतावनी यह है कि पृथ्वी एक दशक में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकती है. इन दोनों तापमानों को अलग करने वाला 0.3 डिग्री सेल्सियस अंतर ही दुनिया को अलग बनाता है. वैज्ञानिकों का मानना है कि दुनिया के तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर करने से जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभावों से बचने में मदद मिल सकती है. इसलिए जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, तेल को त्यागने की जरूरत है. लेकिन भारत जैसे बढ़ते देश के लिए जिसकी लगातार बढ़ती ऊर्जा आवश्यकता है, वह अचानक कोयला नहीं छोड़ सकता. यह कोयला खोदना जारी रखेगा जो लंबे समय में समस्याग्रस्त हो सकता है.”
इसे भी पढ़ें: संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम की एक्सपर्ट से जानें, जलवायु परिवर्तन वैश्विक भूख को कैसे प्रभावित कर रहा है?
श्री रघुनंदन ने कहा कि भारत को अब समुद्र के स्तर में वृद्धि, सार्वजनिक परिवहन में वृद्धि, वन कवर बढ़ाने और भारत द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के भीतर अन्य क्षेत्रों को कवर करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. विशेषज्ञों ने सिफारिश की कि अकुशल कोयला संयंत्रों को बंद करके और नए निर्माण न करके कोयले से दूर जाना भारत के वैश्विक जलवायु लक्ष्य को 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि के अनुकूल बनाने की दिशा में पहला और बहुत महत्वपूर्ण कदम है.