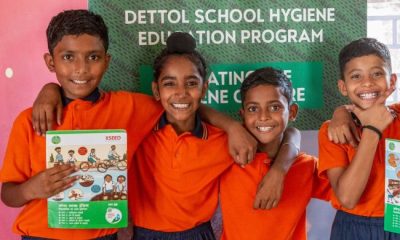नई दिल्ली: दुनिया COVID-19 महामारी के तीसरे वर्ष में है, लेकिन SARS-CoV-2 के नए रूप अभी भी उभर रहे हैं क्योंकि वायरस का लोगों को संक्रमित करना और आगे फैलाना जारी है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, जो इन प्रकारों पर नज़र रखता है, वह है जीनोम सीक्वेंसिंग, जो इनकी विशेषताओं को पहचानने और समझने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है. जीनोम सीक्वेंसिंग का उपयोग वर्षों से वायरस, बैक्टीरिया, पौधों, जानवरों और मनुष्यों जैसे जीवों के अध्ययन के लिए किया जाता रहा है. एनडीटीवी ने टाटा इंस्टीट्यूट फॉर जेनेटिक्स एंड सोसाइटी के निदेशक और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद-सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी (सीसीएमबी) के पूर्व निदेशक डॉ. राकेश मिश्रा के साथ बात की, और जाना कि भारत ने अपनी जीनोम सीक्वेंसिंग क्षमता को कैसे बढ़ाया है और कितना महत्वपूर्ण होगा यह न केवल COVID-19 बल्कि अन्य बीमारियों के प्रकोप से लड़ने में भी मददगार हो सकता है.
इसे भी पढ़ें: कोविड-19 महामारी बनी हुई है पब्लिक हेल्थ अमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न: विश्व स्वास्थ्य संगठन विशेषज्ञ
NDTV: क्या यह SARS-Cov-2 की कुछ अनोखी बात है कि यह इतना बदल रहा है और इसके इतने सारे वेरिएंट हैं?
डॉ. राकेश मिश्रा: ऐसे कई वायरस पहले से ही ज्ञात हैं जो म्यूटेंट होते हैं. SARS-CoV-2 में कुछ भी असामान्य नहीं है. इन विषाणुओं में म्यूटेंट उनकी सर्वाइवल स्ट्रेटेजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है. तो, इस तरह वे नए कैरेक्टर में आते रहते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली से बचते हैं क्योंकि उन्हें बार-बार एक नया होस्ट खोजना पड़ता है. अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें हटा दिया जाएगा. तो, नए वेरिएंट आते रहेंगे. ऐसा इसलिए है क्योंकि एक बार जब हम संक्रमित हो जाते हैं या टीका लग जाता है, तो हम इम्यूनिटी विकसित कर लेते हैं, लेकिन हमें फिर से संक्रमित करने के लिए, वायरस को शरीर में विकसित इम्यूनिटी से लड़ना होगा. वायरस हमेशा अधिक से अधिक लोगों को संक्रमित करने का लक्ष्य रखता है. कोरोनावायरस ने अब यह विशेषता हासिल कर ली है और यह बहुत संक्रामक हो गया है. जीवित रहने के लिए भविष्य के वेरिएंट और भी अधिक संक्रामक होंगे. तो, म्यूटेशन एक बहुत ही प्राकृतिक प्रक्रिया है जो ऐसे वायरस से अपेक्षित है.
इसे भी पढ़ें: क्या हैं नए कोविड वेरिएंट एक्सई के लक्षण: 10 बातें, जो आपको पता होनी चाहिए
NDTV: कोरोनावायरस का प्रकोप अतीत में हुआ है, चाहे वह 2002 में SARS का प्रकोप हो या 2012 में MERS का प्रकोप हो. यह महामारी इन पहले के प्रकोपों से कैसे अलग है.
डॉ. राकेश मिश्रा: कुछ ऐसे कारक हैं जो SARS-CoV-2 को अद्वितीय बनाते हैं. पहला, हमारा व्यवहार बदल गया है. 20 साल पहले की तुलना में, लोगों की गतिशीलता के मामले में ग्रह बहुत छोटा हो गया है. जब हम ट्रेवल करते हैं, तो हम वायरस और संक्रमण भी अपने साथ ले जाते हैं. दूसरा कारक यह है कि यह वायरस पहले के SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) और MERS (Middle East Respiratory Syndrome) की तुलना में कहीं अधिक संक्रामक है. सौभाग्य से, SARS-CoV-2, SARS और MERS जितना घातक नहीं है. क्योंकि SARS-CoV-2 इतनी तेजी से फैलता है कि यह एक महामारी बन गया. पिछले साल नवंबर में, यह पाया गया कि अफ्रीकी देशों में ‘ओमिक्रोन’ नामक एक नया वेरिएंट है और 4-5 सप्ताह के भीतर, वायरस पूरी दुनिया में फैल गया था.
NDTV: पिछले कोरोनावायरस के प्रकोप को कैसे कम किया गया था और हम COVID-19 महामारी को समाप्त करने के लिए संघर्ष क्यों कर रहे हैं, यह तब है जब हमारे पास कई टीके हैं जो रिकॉर्ड समय में विकसित किए गए हैं, जो पहले नहीं थे?
डॉ. राकेश मिश्रा: जब कोई वायरस इन्फेक्शस हो जाता है, तो उसके कई फायदे होते हैं, क्योंकि यह नए रूपों को तेजी से पेश करने में सक्षम होता है. वेरिएंट तभी आते हैं जब वायरस किसी व्यक्ति को संक्रमित करता है और नए म्यूटेशन बनाता है. अधिकांश म्यूटेशन वायरस के लिए उपयोगी नहीं होते हैं और गायब हो जाते हैं लेकिन कुछ जो अधिक संक्रामक होते हैं, वे जीवित रहते हैं और जनता पर हावी होने लगते हैं. जबकि पहले SARS या MERS से संक्रमित व्यक्ति केवल एक या दो लोगों को संक्रमित कर सकता था, वहीं SARS-CoV-2 से संक्रमित व्यक्ति 10 या उससे भी अधिक लोगों को संक्रमित कर सकता है. इस मामले में एक चेन रिएक्शन है.
शुक्र है, हमारे पास डेथ रेट को कंट्रोल में रखने के लिए टीके हैं. टीकों ने लाखों लोगों की जान बचाई है. जबकि टीके संक्रमण को रोकने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन वे बीमारी की गंभीरता को रोकने में सक्षम हैं. साथ ही, चूंकि यह वायरस तेजी से फैलता है और नए वेरिएंट जल्द ही आते हैं, इससे पहले कि हमारा शरीर इससे मुकाबले करने के लिए तैयार हो जाए, नए वेरिएंट हम पर हमला कर देते हैं. ओमिक्रोन का मामला ही लें, तो यह वेरिएंट तेजी से फैला, हालांकि बहुत से लोगों में संक्रमण या वैक्सीन के माध्यम से पहले से ही इम्यूनिटी थी लेकिन फिर भी यह वायरस उस इम्यूनिटी को तोड़ने में सक्षम था.
इसे भी पढ़ें: “मास्क पहनने, हाथ साफ रखने जैसे दिशानिर्देश 31 मार्च के बाद भी जारी रहेंगे” : स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया स्पष्ट
NDTV: जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है और यह रोग के प्रकोप या इसकी रोकथाम में क्या भूमिका निभाता है?
डॉ. राकेश मिश्रा: जीनोम सभी जीवित प्राणियों की आनुवंशिक सामग्री है. कोरोनावायरस के जीनोम आरएनए के रूप में होते हैं जबकि अधिकांश अन्य में उनकी आनुवंशिक सामग्री के रूप में डीएनए काम करता है. पूर्ण सीक्वेंसिंग जीनोम की आनुवंशिक सामग्री का पूरा विवरण है जिसे जीनोम सीक्वेंसिंग कहा जाता है. जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए हम प्रौद्योगिकी और मशीनों की मदद से जीनोम बनाने वाली रासायनिक इकाई को समझते हैं. हम जानते हैं कि इस वायरस में 30,000 अक्षर क्या हैं. अब, जैसे-जैसे वायरस बदलता है, वे परिवर्तन क्रम में जुड़ता जाता है, ऐसे में हम एक वायरस से दूसरे वायरस के बीच के संबंध को समझ पाते हैं, इसी तरह हम व्यक्तियों के बीच उनके डीएनए सीक्वेंसिंग को पढ़कर संबंधों को जान सकते हैं.
वायरस के जीनोम को पढ़कर हम यह पता लगा सकते हैं कि यह कैसे फैल रहा है, यह किस रास्ते पर चल रहा था – क्या यह पहले मुंबई में पाया गया, फिर दिल्ली में आदि. इसके अलावा, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कुछ विशेष वायरस अधिक हानिकारक होते हैं और कुछ कम हानिकारक होते हैं इसलिए यदि हम देखते हैं कि कहीं लोग अचानक बीमार पड़ने लगे हैं, तो हमें यह देखना चाहिए कि कोई नया वायरस आया है या संख्या बढ़ रही है या नहीं. जब हम देखते हैं कि एक नया वेरिएंट आया है, तो हम जानते हैं कि हमें अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी.
एक और महत्वपूर्ण बात जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से एकत्र किए गए आंकड़े दवाओं और टीकों के विकास में मदद कर सकते हैं. COVID-19 के खिलाफ टीके बहुत कम समय में विकसित किए जा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही वायरस की पहचान हुई, इसका क्रम उपलब्ध कराया गया और हफ्तों के भीतर लोगों ने टीकों पर काम करना शुरू कर दिया.
ये भी देखें: कोविड-19: क्या एक्सई वेरिएंट भारत को चौथी लहर की ओर ले जा सकता है?
NDTV: जीनोम सीक्वेंसिंग के मामले में दुनिया के अन्य देशों की तुलना में भारत की क्षमताएं किस प्रकार की हैं? जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भारत के पास किस प्रकार का बुनियादी ढांचा है?
डॉ. राकेश मिश्रा: हमारे देश में जीनोम सीक्वेंसिंग की क्षमता उचित है, विशेष रूप से SARS-CoV-2 के जीनोम के सीक्वेंसिंग के लिए. हमने इसके लिए जबरदस्त क्षमता विकसित की है. इसलिए SARS-CoV-2 की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए क्षमता कोई समस्या नहीं है. देश में लगभग 12 स्थान ऐसे हैं जहां प्रतिदिन हजारों जीनोमों की सीक्वेंसिंग की जाती है और सैकड़ों अन्य केंद्र हैं, जहां छोटे पैमाने पर सीक्वेंसिंग की जा रही है. एकमात्र तार्किक चुनौती यह है कि हमें उन रसायनों का आयात करना पड़ता है जिनका उपयोग जीनोम सीक्वेंसिंग मशीनों को चलाने के लिए किया जाता है जिनकी लागत बहुत अधिक होती है. यदि हम जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए अपने स्वयं के रसायनों को आवश्यक बना सकें, तो यह सस्ता हो जाएगा. वर्तमान में, प्रत्येक सीक्वेंसिंग की लागत 3,000-5,000 रुपए आती है.
NDTV: महामारी से पहले भारत जीनोम सीक्वेंसिंग का उपयोग किस लिए कर रहा था और यह नीतिगत निर्णय कैसे चला रहा था?
डॉ. राकेश मिश्रा: हम वर्षों से लोगों का अध्ययन करने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग का उपयोग कर रहे हैं. उदाहरण के लिए, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च- सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि 70,000 साल पहले, अंडमान के लोग अंडमान और निकोबार तक पहुंचने के लिए जलमार्ग का उपयोग करके अफ्रीका से आए थे. तो, यह जीनोम सीक्वेंसिंग के कारण स्थापित किया गया था. इस तरह हम यह भी पता लगा सकते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप कैसे बसा हुआ था. इसके अलावा, भारत में 5,000 से अधिक जातीय समूहों की एक समृद्ध विविधता है. हम उन्हें न केवल उनकी विशेषताओं से बल्कि उनके जीन से भी अलग कर सकते हैं. जीनोम सीक्वेंसिंग अब यह तय करने में अत्यंत उपयोगी हो गई है कि हमें किस प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं और हमें विशेष रूप से कैंसर और मानसिक रोग के लिए किस प्रकार का ट्रीटमेंट करना चाहिए. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 50 प्रतिशत से अधिक आनुवंशिक व्यक्तियों में दवाएं काम नहीं करती हैं. इसलिए, यदि हम आनुवंशिक जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हैं, तो हम बता सकते हैं कि कौन सी दवा किस व्यक्ति के लिए उपयोगी होगी और हम बिना अनावश्यक उपचार और विषाक्तता से भी बच सकते हैं. जीनोम सीक्वेंसिंग का उपयोग मवेशियों और फसलों की विविधता में सुधार के लिए भी किया जाता है.
ये भी देखें: कोविड-19 वायरस के प्रसार पर प्रतिबंधों में ढील का असर
NDTV: भारत में COIVD-19 के प्रकोप के बाद से जीनोम सीक्वेंसिंग कैसे विकसित हुई है?
डॉ. राकेश मिश्रा: हमें जीनोम सीक्वेंसिंग विकसित करने की आवश्यकता नहीं है, तकनीक पहले से मौजूद है. बात बस इतनी है कि अधिक से अधिक लैब ने इसका उपयोग करना शुरू कर दिया है क्योंकि अब इसके लिए छोटी मशीनें भी उपलब्ध हैं जिनकी कीमत 2 लाख रुपए है. बड़ी मशीनों की कीमत 9 करोड़ तक हो सकती है. छोटी मशीनों का उपयोग दूरस्थ स्थानों पर किया जा सकता है और इन्हें स्थापित करने के लिए अधिक बुनियादी ढांचे की आवश्यकता नहीं होती है. इससे स्थानीय स्तर पर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए क्षमता निर्माण में मदद मिली है. इतिहास में पहले कभी भी हमने निगरानी उद्देश्यों के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग का इतना अधिक उपयोग नहीं किया है.
NDTV: COVID-19 के लिए टेस्ट किए जा रहे सैम्पल की कितना प्रतिशत सीक्वेंसिंग की जा रही है और क्या यह किसी भी स्थापित अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क के अनुसार है?
डॉ. राकेश मिश्रा: पहले हम पर्याप्त सीक्वेंसिंग नहीं कर रहे थे. लेकिन दूसरी लहर के दौरान हमने जीनोमिक विविधताओं की निगरानी के लिए मल्टी-प्रयोगशाला, मल्टी-एजेंसी, अखिल भारतीय नेटवर्क की स्थापना, NSACOG (भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम) के साथ इसे और अधिक संगठित तरीके से करना शुरू कर दिया. तीसरी लहर के दौरान हम काफी सीक्वेंसिंग कर रहे थे. एक मानदंड जो हम कह सकते हैं कि हमने देखा है वह यह है कि हम इस बात से सावधान नहीं हुए हैं कि एक नया वैरिएंट आया और इसको लेकर जल्दी कदम नही उठाए गए.
हमें सीक्वेंसिंग में ढील नहीं देनी चाहिए. जब केस कम होते हैं तो हम थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं. लेकिन यह वह समय है जब हमें वास्तव में और अधिक सीक्वेंसिंग करनी चाहिए, क्योंकि अब जहां भी हमें नए वेरिएंट मिलते हैं, हमें वहां पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और जहां ये कम होते हैं वहां वायरस को तुरंत दबा देना चाहिए, न कि इसके फैलने का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि तब यह नियंत्रण से बाहर हो जाता है. अगर हम देखते हैं कि कहीं लोग ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं तो अस्पताल आने वाले हर व्यक्ति की सीक्वेंसिंग की जानी चाहिए. जीनोम सीक्वेंसिंग स्ट्रेटेजी की योजना और कार्यान्वयन में ढील नहीं दी जानी चाहिए.
इसे भी पढ़ें: दिल्ली में कोविड-19 मामलों में तेजी, विशेषज्ञों ने कहा- “मास्क पहनें, घबराएं नहीं”
NDTV: इस महामारी से क्या बड़ी सीख मिली है?
डॉ. राकेश मिश्रा: महामारी ने हमें एहसास कराया है कि संक्रामक रोग कितने महत्वपूर्ण हैं. हमने देखा है कि सबसे ज्यादा नुकसान विकसित देशों में हुआ है. हम अब संक्रामक रोगों को नजरअंदाज नहीं कर सकते. एक और सीख यह है कि यद्यपि हम कहते हैं कि हम एक सिविलाइज्ड वर्ल्ड हैं, लेकिन ये देखने वाली बात है कि कैसे एक देश में अधिक टीके हैं वहीं एक पूरे महाद्वीप में कोई भी टीका नहीं है. यह हम सभी के लिए शर्म की बात है. साथ ही यह दुनिया के लिए सुरक्षित भी नहीं है. इसलिए, वैक्सीन इक्विटी अत्यंत महत्वपूर्ण है. मेरे लिए एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अब हमें यह महसूस करना चाहिए कि यह ग्रह सभी प्राणियों का है न कि सिर्फ इंसानों का. सभी महामारियां जंगल से आती हैं क्योंकि हम उनके स्थान का अतिक्रमण करते हैं, हम उन्हें परेशान करते हैं. हमें सीमित संसाधनों के दायरे में रहना सीखना होगा. हमें अपनी वर्तमान स्वास्थ्य प्रणाली को भी देखने और इसे मजबूत करने की आवश्यकता है.
इसे भी पढ़ें: Opinion: कोविड-19 के खिलाफ अपनी प्रतिरोधक क्षमता को करें मजबूत, मनाएं हेल्दी नया साल 2022
अब आप बनेगा स्वस्थ इंडिया हिंदी पॉडकास्ट डिस्कशन सुन सकते हैं महज ऊपर एम्बेड किए गए स्पोटिफाई प्लेयर पर प्ले बटन दबाकर.
हमें एप्पल पॉडकास्ट और गूगल पॉडकास्ट पर फॉलो करें. साथ ही हमें रेट और रिव्यू करें.